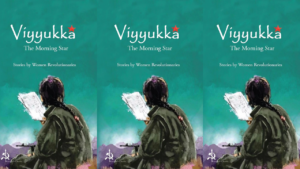
शरजील इमाम: इस्लामी आधुनिकतावाद, जिन्ना, लोकतंत्र और भारत में मुसलमानों का व्यवस्थागत बहिष्करण

पाँच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद ज़मानत से वंचित, आईआईटी से स्नातक और जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम का मुक़दमा अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। उनके वकील के अनुसार, आरोपों पर बहस अभी जारी है, लेकिन उसके पूरा होने की कोई स्पष्ट संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आती। इस खुले पत्र में शरजील इमाम अपने प्रारंभिक वर्षों, शाहीन बाग़ आंदोलन और तौहीद (एकेश्वरवाद) की चर्चा करते हैं जिससे उन्हें संबल मिलता है।
हमें कभी भी किसी शख्स के बारे में सिर्फ उसके विरोधियों की बातों पर यक़ीन करके राय नहीं बनानी चाहिए, खासतौर पर तब, जब वह हमारा हमसफ़र हो। मेरे मामले में भी, भाजपा और उनके समर्थकों द्वारा चालाकी से फैलाई गई एक छोटी सी वीडियो क्लिप की वजह से, 2019 में, केंद्र सरकार के नए नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ मेरा शाहीन बाग और जामिया की सड़कों पर एक महीने तक किया गया संघर्ष, और दस साल की मेहनत से किये गए मेरे शोध और लेखन को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैंने ‘कांग्रेसी राष्ट्रवाद’ का शिकार मुहम्मद अली जिन्ना के विचारों पर भी गंभीरता से सोचने की कोशिश की।
दरअसल, जिन्ना की बजाय नेहरू ने 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान को नाकाम किया था, जबकि सारी पार्टियां उस पर सहमत हो चुकी थी। (देखे, मौलाना आज़ाद की ‘India Wins Freedom’, और आकार पटेल की ‘The Constitution that Wasn’t’ – या ‘A Muslim Man’s Vision of Independent India’, National Herald 26, January 2025).
जिन्ना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, खासकर तब, जब कोई बातचीत सत्ता के विकेंद्रीकरण, अल्पसंख्यक अधिकारों और समुदाय के अधिकारों पर हो रही हो। मेरे द्वारा किया गया जिन्ना का उल्लेख इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए। पार्थसारथी गुप्ता के शब्दों में मेरी अपील है कि “दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था और एक परिसंघीय साझेदारी की स्थापना” की जाए। (देखें गुप्ता का लेख Identity Formation and Nation States, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, पटियाला, 1998)। वे आगे लिखते हैं: “अगर हमारे अपने देश में हम 1935 के भारत शासन अधिनियम (GOI Act, 1935) की केंद्रीयतावादी प्रवृत्तियों को छोड़ दें और भारत को राज्यों का एक वास्तविक संघ बना दें, तो हम अपने पड़ोसी देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) के सदस्य देशों को लोगों का एक वास्तविक परिसंघ बनाने की स्थिति में आ सकते हैं…”।
बेशक, आप मुझसे इत्तेफ़ाक न रखते हो, लेकिन अगर आप मेरे बारे में राय उस झूठी तस्वीर के आधार पर बनाएंगे, जो ट्रोल आर्मी आपको दिखाना चाहती है, तो ये नाइंसाफी होगी। अतः, मुझे सनकी कहना या बीजेपी एजेंट करार देना, केवल इसलिए क्योंकि मेरे विरोधी मेरे विचारों को पचा नहीं पाते ,यह भी उतना ही गलत है। “प्रगतिशील” माने जाने वाले मीडिया और राय–निर्माताओं के एक हिस्से (चाहे वे मुस्लिम हों या ग़ैर–मुस्लिम) ने मुझे चुप कराने की कोशिश की और शाहीन बाग में पहले दिन से लेकर 18 वें दिन तक हमारे अथक और निर्णायक योगदान को मिटाने की कोशिश की। मेरा आशय उन किताबों से है जो शाहीन बाग पर लिखी गई हैं। इनमें मेरा, आसिफ़ मुज्तबा, अफ़रीन फ़ातिमा या अन्य साथियों का ज़िक्र तक नहीं है। यह साफ दर्शाता है कि यह तबका या तो बेईमानी से काम कर रहा है या बौद्धिक रूप से दीवालिया हो चुका है। लेकिन शुक्र है कि आज के दौर में तथ्यों को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस यह बता ही रहा हूं। ख़ुदा पर यक़ीन और अपने लोगों की मुहब्बत मेरे लिए पर्याप्त है।
अक़ीदत (आस्था) के बारे में
ग्राम्शी ने कहा था – “मैं अपनी बुद्धि के कारण निराशावादी हूँ और अपनी इच्छाशक्ति के कारण आशावादी।” मेरे मामले भी यह बात सही बैठती है, हालांकि मैं इसे कुछ इस तरह कहना पसंद करूंगा – मैं अपनी बुद्धि के कारण निराशावादी हूँ और अपनी अक़ीदत के कारण आशावादी। कई लोगों के लिए “इच्छाशक्ति” और “अक़ीदत ” एक ही चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे उन लोगों के लिए जो इस्लामी यक़ीन में पले–बढ़े हैं, “इच्छाशक्ति” की कोई अहमियत नहीं, अगर वह ख़ुदा में यक़ीन और मेरे लिए उसकी उसकी योजना पर “अक़ीदत” से जुड़ी न हो। एक महान “इच्छाशक्ति” है – ‘ख़ुदा की इच्छाशक्ति’, और जब तक हमारी छोटी–छोटी “इच्छाशक्तियों” में उस “महान इच्छाशक्ति” पर यक़ीन नहीं होता, तब तक वे न कोई अर्थ रखती हैं, न उम्मीद। यह एक चीज़ है जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते, केवल उस पर यक़ीन रख सकते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो, इतिहास “अज्ञेय” है, वर्तमान “अज्ञेय” है, और भविष्य की दिशा भी “अज्ञेय” ही है। हमारे पास जो कुछ है, वे या तो अधूरे अनुमान हैं या कई बार पूरी तरह से ग़लत धारणायें हैं। किसी के योगदान का अर्थ समझना, या ख़ुदा की वृहद योजना में, अपनी जगह को समझना अक़ीदत के बिना असंभव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही जीवनकाल में परिवर्तन देखने के लिए उतावले रहते हैं। उन्हें लगता है कि क्रांति तो बस होने ही वाली है। लेकिन इस सोच की समस्या यह है कि इसमें बुनियादी बदलाव के लिए जो धैर्य चाहिए, वह नदारद रहता है। ऐसा धैर्य यानि आत्मविलोपी धैर्य, सिर्फ अक़ीदत से ही आ सकता है। ख़ुदा में यक़ीन ने ही मुझे इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, मुझे जेल में टिके रहने की ताक़त दी। मेरी ज़िंदगी और मेरे काम को मैं दशकों में नहीं, शताब्दियों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखता हूं, वह भी सिर्फ और सिर्फ ख़ुदा में मेरे यक़ीन का परिणाम है।
अब तक मैं पाँच साल जेल में बिता चुका हूं। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि ये साल मेरे जीवन के सबसे उत्पादक साल रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस दौरान मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ीं, बल्कि इसलिए भी कि मैं बहुत से राजनीतिक बंदियों से मिला, छह महीने असम के लोगों के साथ रहा, और पिछले चार साल से दिल्ली और हरियाणा के लोगों के साथ रह रहा हूं। यह सब कुछ मेरे लिए सीखने का एक अनुभव रहा है।
मैं इस्लामी आधुनिकतावाद का एक छात्र हूं। जमालुद्दीन अफ़ग़ानी तथा मिस्र के मोहम्मद अब्दुह जैसे विद्वानों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। हमारे अपने अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इक़बाल, मौलाना आज़ाद, और ईरानी इन्क़लाबी अली शरियाती ने भी मेरे राजनीतिक और धार्मिक सोच को आकार दिया है। इन्हीं लोगों की प्रेरणा से एक इंजीनियरिंग स्नातक होने के बावजूद मैंने इस्लाम और इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया।
मैं बिहार के पटना और जहानाबाद में एक पारंपरिक मध्यमवर्गीय परिवार में पला–बढ़ा हूं। मेरे अब्बू एक स्थानीय राजनेता थे। उन्होंने सन 2000 में कुर्था से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2005 में उन्हें जहानाबाद सीट से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का टिकट मिला। वह दोनों चुनाव हार गए। कुर्था में तीसरे स्थान पर रहे और जहानाबाद में दूसरे। लेकिन इन चुनावों में उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके पीछे कई राज्य विधानसभा सीटों पर लगभग 10 प्रतिशत वोट बैंक है, और वह भी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम आबादी मात्र 10-12 प्रतिशत है। इससे उन्हें जेडीयू में एक राजनीतिक पकड़ मिली जो 2005 से लगातार बिहार की सत्ता में बनी हुई है। मेरे अब्बू के इस बिखरे हुए वोट बैंक ने ही मुझे पहली बार सरल बहुमत प्रणाली [फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP)] की खामियों का एहसास कराया, और इसने मुझे अनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया।
जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है, सरल बहुमत प्रणाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) में किसी भू–भाग को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, और हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे सबसे अधिक वोट मिले हों। सबसे ज्यादा मत पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसे केवल 20 प्रतिशत वोट मिले हों। यही वह प्रणाली है, जिसके कारण कोई पार्टी कुल मतों के लगभग एक–तिहाई हिस्से के साथ भी विधानसभाओं में दो–तिहाई बहुमत प्राप्त कर सकती है। भारत की संविधान सभा की बहसों में भी इस मुद्दे पर असहमति देखी गई थी, विशेषकर तब, जब कांग्रेस पार्टी ने पृथक निर्वाचक क्षेत्रों (separate electorates) को समाप्त कर दिया। जबकि, कुछ मुसलमानों ने उस समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की माँग की थी। हालांकि, यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की एक गंभीर खामी यह थी कि यहां हिंदू, मुसलमानों को वोट नहीं दे सकते थे और मुसलमान हिंदुओं को नहीं। शायर, स्वतंत्रता सेनानी और FPTP प्रणाली के प्रखर विरोधियों में से एक हसरत मोहानी, का तर्क था कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों (joint electorates) के चलते मुसलमानों का प्रतिनिधित्व धीरे–धीरे समाप्त हो जाएगा। इसका विकल्प था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसमें पार्टी को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें मिलतीं। इसमें मुसलमान हिंदुओं को वोट दे सकते थे और हिंदू मुसलमानों को। और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को पूरी तरह खामोश नहीं किया जा सकता।
आईआईटी में बिताए मेरे साल
2006 में, जब मैं 18 साल का था, मैंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) पास किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए दाख़िला लिया। इसके साथ–साथ मेरी दिलचस्पी अरबी और फ़ारसी में धार्मिक साहित्य पढ़ने में भी थी। मैं तब तक इस्लामी आधुनिकतावाद (Islamic Modernism) से परिचित नहीं हुआ था, लेकिन इस्लामी इतिहास का गहन अध्ययन भी कर रहा था। आईआईटी के दूसरे वर्ष में साहित्य की एक कक्षा में, जब प्रोफेसर ने विकासवाद के बारे में पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने आपत्ति की और कहा कि विकासवाद महज़ एक “सिद्धांत” है, कोई सिद्ध विज्ञान नहीं।
आईआईटी के प्रोफेसर जेएनयू के प्रोफेसरों जैसे थे। उन्होंने मुझे चुप नहीं कराया, बल्कि कहा कि मैं इस पर एक प्रस्तुति तैयार करूं। अगले हफ्ते, Literature 101 की कक्षा में लगभग 200 छात्रों के सामने, मैंने अपनी प्रस्तुति दी। जिसमें मैंने उन ईसाई छद्म–विज्ञानियों की टिप्पणियां पेश की थीं, जिन्हें मैंने कुछ इस्लामी किताबों में विकासवाद का खंडन करते हुए पाया था।
मेरी आधे घंटे की प्रस्तुति सुनने के बाद प्रोफेसर ने मेरे प्रयास की सराहना की, लेकिन साथ ही कुछ किताबें पढ़ने की सलाह भी दी। हालांकि, इन किताबों से कहीं ज़्यादा जिसने मुझे विकासवाद को समझने में मदद की, वह थे – 20वीं सदी के शायर–फ़िलॉसफ़र– इक़बाल। दक्षिण एशिया के मुसलमानों के बीच जिन्हें अत्यंत सम्मान के साथ याद किया जाता है। आम जनमानस में इक़बाल की छवि बस उस शायर की है जिसने “सारे जहाँ से अच्छा“ लिखा था। लेकिन एक दार्शनिक के रूप में इक़बाल को लगभग पूरी तरह से नज़रंदाज़ किया गया।
इक़बाल ने ही थे मुझे हेनरी बर्गसों और उनकी किताब Creative Evolution से परिचित कराया। इक़बाल ही ने मुझे कार्ल मार्क्स और उनकी कैपिटल से भी परिचित कराया। इक़बाल ने इन दोनों विचारकों की आलोचना की, लेकिन गहराई और सम्मान के साथ। मेरी बात यह है कि पूंजीवाद के बारे में मेरी आँखें मार्क्स ने नहीं खोलीं, और विकासवाद के प्रति आदर भाव डार्विन ने नहीं जगाया, बल्कि इक़बाल ने मुझे इन चीज़ों को समझने का रास्ता दिखाया। इसकी वजह भी सीधी है, बीसवीं सदी के ज़्यादातर विचारकों ने इन मुद्दों को केवल भौतिकवादी (materialist) ढंग से देखा, जिसने मुझे (उत्तरों की तलाश में एक जिज्ञासु लेकिन अक़ीदतमंद मुस्लिम युवा को) इनसे दूर कर दिया। (मैं साम्यवाद–विरोधी नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि हालिया मानव इतिहास, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद की कुरूप विचारधाराओं के विरुद्ध संघर्ष, और अंधविश्वास के खिलाफ़ जो ठोस राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण कम्युनिस्टों ने दिए, भविष्य के विचार–निर्माण में उन्हें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या वहां आती है जहाँ कम्युनिस्ट यह दावा करते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक विज्ञान है, जबकि भौतिकवादी अस्तित्वमीमांसा (materialist ontology) को भौतिक विज्ञान ने तो एक सदी पहले ही त्याग दिया था। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए देखें मेरा लेख : Worldview in a Cell: A Muslim Political Prisoner’s Insight)।
हालांकि, विज्ञान ने 20वीं सदी की शुरुआत में ही नियतिवादी भौतिकवाद (deterministic materialism) को त्याग दिया था, लेकिन राजनीतिक विचारधाराएं अब भी न्यूटन युग की भाषा और सोच का ही अनुसरण करती हैं। यहीं पर इक़बाल जैसे चिंतक एक नया रास्ता खोलते हैं – ऐसा रास्ता जो यह भ्रम नहीं फैलाता कि हमने सब कुछ जान लिया है या यह कि हम सब कुछ जानने की ओर अग्रसर हैं। यहीं पर “अक़ीदत” एक व्यक्ति और समुदाय के विकास के लिए नींव का पत्थर बनकर उभरती है। इक़बाल उन विरले दार्शनिकों में से थे जिन्होंने न्यूटन के बाद के वैज्ञानिक ज्ञान को अक़ीदत के सवाल के साथ संश्लेषित करने की कोशिश की। निश्चित रूप से, मैं यहां जिन बातों की ओर इशारा कर रहा हूं, वे हैं– 20वीं सदी की भौतिकी की क्रांतियों (सापेक्षता का सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी) से उत्पन्न अस्तित्वमीमांसा संबंधी (ontological) और ज्ञानमीमांसा संबंधी (epistemological) सवाल। इन सिद्धांतों ने न सिर्फ भौतिकवादी चिंतन धाराओं की पारंपरिक दार्शनिक मान्यताओं को तोड़ा, बल्कि अधिकांश धार्मिक चिंतन धाराओं को भी झकझोर दिया।
भौतिकवाद (materialism) और नियतिवाद (determinism) की आलोचना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का ज़िक्र करना आवश्यक है। क्वांटम भौतिकी के संस्थापक वैज्ञानिकों में से एक वर्नर हाइज़ेनबर्ग की इस किताब को सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए – Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science। रहस्यवादी विचारों में समर्थन के लिए क्वांटम भौतिकी के एक अन्य संस्थापक वैज्ञानिक एरविन श्रोडिंगर की दो किताबें What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell और Mind and Matter पढ़ें. और आगे बढ़ते हुए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मैक्स जैमर की किताब The Conceptual Development of Quantum Mechanics का विशेष रूप से अध्याय “The Philosophical Background of Nonclassical Interpretations” भी पढ़ें। इससे आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह डेनमार्क के 19वीं सदी के ईसाई दार्शनिक सोरेन कीर्केगार्द जो अस्तित्ववाद (existentialism) और नव–रूढ़िवादी धर्मशास्त्र (neo-orthodox theology) के अग्रदूत माने जाते हैं – का प्रभाव नील्स बोर पर पड़ा, जो क्वांटम भौतिकी के अग्रदूतों में एक थे।
इसके साथ–साथ, मैं यह भी सुझाऊंगा कि आप कुर्ट गोडेल (Kurt Gödel) – जो 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं—की 1946 से 1966 के बीच की चिट्ठियाँ अवश्य पढ़ें। इन पत्रों में उनकी ईसाई एकेश्वरवादी (monotheistic) यक़ीन का स्पष्ट विवरण मिलता है। इनका सार आप हाओ वांग (Hao Wang) के निबंध A Logical Journey: From Gödel to Philosophy (1996) में पढ़ सकते हैं। गोडेल के सापेक्षता सिद्धांत (General Relativity) से जुड़ाव को समझने के लिए पढ़ें – Gödel Meets Einstein: Time Travel in the Gödel Universe। इस्लाम की प्रारंभिक बौद्धिक प्रतिक्रिया को विशेष रूप से सापेक्षतावाद (relativity) और विकासवाद (evolution) के सन्दर्भ में समझने के लिए इक़बाल की निम्न किताबों से होकर गुजरना होगा – The Reconstruction of Religious Thought in Islam (1930), Javid Nama (The Book of Eternity, 1932), Saqi Nama (The Book of the Winebringer, 1935)।
मैं इन पन्नों को संदर्भों से भर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे विचारों की गंभीरता से जाँच करें और खुद उनसे संवाद करें। मेरे शब्द महज प्रलाप नहीं हैं, बल्कि वे मेरे विज्ञान, धर्मशास्त्र और अध्ययन से उपजे सवाल हैं। इन सिद्धांतों और विचारों के बारे में कहने और विश्लेषित करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इस समय मैं यह नहीं कर सकता। फिर भी, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इन पर और विस्तार से लिख सकूं।
आईआईटी बॉम्बे से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक मैंने मन बना लिया था कि मुझे आगे दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना है। 2009 में, कोपेनहेगन में मेरी समर इंटर्नशिप ने मुझे पश्चिमी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वातावरण और स्कैंडेनेवियाई कल्याणकारी राज्यों (welfare states) के मॉडल से भी थोड़ा परिचित कराया। इन्हीं अनुभवों पर मेरी एक लंबी बातचीत हुई अमिताभ सान्याल से, जो मेरे पसंदीदा प्रोफेसर और प्रोजेक्ट गाइड थे। उन्होंने मुझे दर्शनशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे एक किताब भेंट की – आर्थर कोएस्टलर की The Sleepwalkers।
इतिहास की ओर
मैंने अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी ने कहा कि दर्शनशास्त्र में पीएचडी में दाख़िला लेने के लिए मेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं मिस्र जाकर अल–अज़हर विश्वविद्यालय में इस्लामिक धर्मशास्त्र (Islamic Theology) और अरबी भाषा का अध्ययन करूंगा, लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग (Arab Spring) आ गया और मेरी योजना ठप पड़ गई। मैंने तब बैंगलोर में एक कंपनी का प्लेसमेंट ऑफर स्वीकार कर लिया और कॉर्पोरेट नौकरी शुरू कर दी। साथ ही साथ, मैं दर्शनशास्त्र और इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करता रहा। 2012 में, मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र में एमफिल/पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया। मैं साक्षात्कार तक पहुंच गया जहाँ फैकल्टी ने मेरे प्रयास की सराहना की, लेकिन कहा कि चूँकि मेरे पास शोध प्रस्ताव नहीं है, इसलिए अगले वर्ष दोबारा आवेदन करूं। लेकिन तब तक मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैंने दर्शन से एक कदम हटकर इतिहास की ओर रुख कर लिया।
विज्ञान की पृष्ठभूमि से आने के कारण मैं हमेशा एक अंतर्द्वंद्व में जीता था। जैसा कि मैंने पहले कहा, बीसवीं सदी की भौतिकी धार्मिक या ग़ैरधार्मिक, दोनों के लिए एक दार्शनिक विस्फोटक सामग्री बन चुकी थी। लेकिन मेरे लिए यह जटिलता और भी गहरी थी क्योंकि मैं उस समुदाय से आता हूँ जो विभाजन का शिकार रहा है, और जो बहुसंख्यकवादी राजनीति और हिंसा की निरंतर मार झेलता रहा है। मेरे पिता, जो खुद एक राजनेता थे, ने ऐसी ताक़तों के खिलाफ़ जीवन भर संघर्ष किया। इसका असर मेरे रोज़मर्रा के जीवन और सोच पर बेहद गहराई से पड़ा। दक्षिण एशियाई इतिहास और उसकी दरारें मेरी रोज़मर्रा की चेतना का हिस्सा थीं। 2011 में मैंने जर्मन भाषा सीखनी शुरू की। 2013 तक मैं बीसवीं सदी के जर्मनी और फासीवाद के इतिहास में पूरी तरह डूब चुका था। यहीं से मेरा झुकाव इतिहास की ओर पूरी तरह से हो गया। मुझे यह अहसास हो गया कि मानव अस्तित्व की प्रकृति, भारत में जातिवाद, राष्ट्रवाद का उदय, बहुसंख्यकवाद और विभाजन व अल्पसंख्यकों के अधिकारों से सम्बंधित दार्शनिक–सामाजिक–राजनीतिक सवालों के जिन उत्तरों को मैं तलाश रहा था, उनकी जड़ें इतिहास में थीं।
जल्दी ही मैंने कॉरपोरेट जीवन को अलविदा कहा और जेएनयू में आधुनिक इतिहास में मास्टर्स करने के लिए दाख़िला ले लिया। मुझे एक पार्ट–टाइम नौकरी मिली जिससे हर महीने ₹25,000 मिलते थे। यह मेरी पिछली तनख़्वाह का एक छोटा–सा हिस्सा था। लेकिन ठीक इसके बाद ही, त्रासदी ने दस्तक दी। जनवरी 2014 में मेरे अब्बू को पेट के कैंसर का पता चला। मेरा दूसरा और तीसरा सेमेस्टर दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में बीता। मैंने एक बार अब्बू से पूछा – “क्या मुझे जेएनयू छोड़कर फिर से कोई कॉरपोरेट नौकरी कर लेनी चाहिए?” उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा “तुम्हारे पैसे मुझे नहीं बचा पाएंगे।” मेरे अब्बू, भले ही एक प्रभावशाली राजनेता थे, सामान्यतः घर का ख़र्च किसी तरह चला पाते थे। उनकी कुल संपत्ति थी – दो गाड़ियाँ, दो राइफलें, और एक दुकान। उनके नाम कोई मकान नहीं था। उस मुश्किल घड़ी में मेरे मामा आगे आए। उन्होंने इलाज़ का सारा खर्च उठाया। अगर वह न होते, तो शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती और नौकरी करनी पड़ती। मैं उनका कर्ज़ कभी चुका नहीं पाऊंगा। (वे राज्य सरकार में इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं।)
मेरी माँ हमेशा मेरे अब्बू की एक धैर्यवान और त्यागमयी जीवनसाथी रही थीं। उन्होंने चाहा कि मैं अपना पुराना कॉरपोरेट कैरियर फिर से शुरू करूँ। उन्होंने अब्बू से भी कहा, “उसे समझाइए, वह वापस चला जाए।” लेकिन मेरे अब्बू ने माँ से कहा: “उसे जहां है वहीं रहने दो। वह हमारे संघर्षों का इतिहास लिखेगा।” मई 2014 में, जब मेरे अब्बू अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए टीवी पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा – “शरजील, तुम्हें भारत छोड़ देना चाहिए। अमेरिका जाओ, वहाँ पढ़ाई करो। अगर यहाँ रुकोगे, तो राजनीति में आओगे। संघर्ष होगा… और वे तुम्हें जेल भेज देंगे।” मैंने तब इसे अपने अब्बू का आत्मीय डर और स्नेह समझा। सोचा कि वे मुझे बचाना चाहते हैं क्योंकि वे खुद शायद ज़्यादा दिन मेरे साथ न रह पाएँ। मैं तब बहुत भोला नौजवान था। दरअसल, वह दुनिया को मुझसे बेहतर समझते थे। वह मुझे भी मुझसे बेहतर समझते थे। उन्हें पता था कि मैं ज़िद्दी हूँ, और अपने विचारों को लेकर अडिग भी। कि मैं एक दिन इस उभरती हुई फासीवादी व्यवस्था से सीधा टकरा जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वह मुझे कभी रोकते, लेकिन वह यह सब पहले से देख रहे थे।
उस साल मैं शायद ही कभी कक्षाओं में उपस्थित रह पाया। लेकिन अस्पताल में ही मैंने ट्यूटोरियल लिखे, सॉफ्टवेयर बनाए (छोटी सी तनख़्वाह भी उस समय बहुत मायने रखती थी), और अस्पताल में अपने अब्बू को किताबें पढ़कर सुनाता रहा। मुझे अब भी याद है, मैं ईरानी क्रांति पर एक किताब पढ़ रहा था, और वे सुनते हुए अपने युवाकाल की स्मृतियों के साथ उस पर टिप्पणी करते जाते थे। नवंबर में वह इस दुनिया से चले गए।
मैंने अगला सेमेस्टर यानि चौथा सेमेस्टर उदासी और शोक में गुज़ार दिया। जेएनयूमें यह मेरा सबसे ख़राब सेमेस्टर था। (इस संदर्भ में विशेष रूप से मैं प्रोफेसर जानकी नायर से क्षमाप्रार्थी हूँ। मैंने उनका एक कोर्स और एक सेमिनार लिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया। सिवाय इसके कि मैंने टीपू सुल्तान की फ़ारसी डायरी पूरी पढ़ डाली।)
मेरे अब्बू की सीख
दुबारा अब्बू पर लौटें तो मैंने उनसे दो अहम बातें सीखी। पहली, कि विभाजन के कारण भारतीय राजनीति में मुसलमानों का योजनाबद्ध बहिष्करण शुरू हुआ। और कि जिन्ना का केंद्रीकरण के विरोध में और एक सच्चे संघीय ढांचे व अल्पसंख्यक अधिकारों की माँग में जो तर्क था, वह सही था। और दूसरी, कि यदि लोकतंत्र में चुनने के लिए सिर्फ एक ही पक्ष बचे, तो वह लोकतंत्र नहीं रहता। इसीलिए, वह हमेशा कहते थे कि JDU और RJD दोनों पार्टियों को मजबूत और परस्पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। अन्यथा, अगर राजनीतिक परिदृश्य का एक कोना भाजपा के लिए खुला छोड़ दिया जाये और जहाँ कोई मज़बूत विपक्षी नेता या दल उन पर अंकुश लगाने के लिए मौजूद न हो, तो चाहे RJD और उसके गठबंधन कितने भी अच्छे क्यों न हों, मुसलमान उनके वोटर नहीं रहेंगे, बल्कि उनके “ग़ुलाम” बनकर रह जाएँगे।
विभाजन और जिन्ना से जुड़ा पहला सबक, जो मैंने अपने अब्बू से सीखा था, उसने मुझे उस सैद्धांतिक खोज की ओर धकेला जिसे मैं आज भी आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन चुनावी राजनीति से जुड़ा दूसरा अधिक व्यवहारिक सबक, अधिक स्पष्ट और जरूरी हो गया क्योंकि पिछले एक दशक में, भारत के लगभग हर हिस्से में मुसलमानों की राजनीतिक एजेंसी छिन चुकी है। केवल तमिलनाडु और केरल, और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और बिहार ही अपवाद हैं। यहाँ तक कि बंगाल में भी, अब भाजपा के उभार के बाद हमारे पास चुनने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं है।
मेरे अब्बू के इन्हीं दो सबक के आधार पर मैंने पढ़ना, शोध करना और उन लोगों को खोजना शुरू किया जो इन्हीं विषयों से जुड़े हुए हैं। मेरे MPhil और PhD, दोनों का विषय है – भारतीय मुसलमानों पर होने वाली हिंसा। क्यों यह जिज्ञासा आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति में सबसे ज़रूरी और प्रासंगिक बन गई है? मुसलमानों की राजनीतिक एजेंसी का खात्मा महज इत्तेफाक़ नहीं है। यह एक व्यवस्थागत और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जिसका सबसे जहरीला रूप 1990 के बाद सामने आया क्योंकि इसी समय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के कई वैश्विक और स्थानीय कारक एक ख़ास तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए।
केवल समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करना पर्याप्त नहीं है। हर चीज़ को सिर्फ़ वर्ग में समेट देना भी समस्यामूलक है। भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की राजनीतिक एजेंसी की बहाली के लिए, आगे का रास्ता तभी निकलेगा जब यह मान लिया जाए कि इस पूरी व्यवस्था में बदलाव लाना ज़रूरी है। इसी कारण से जिन्ना आज 1947 से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं। क्योंकि जिन्ना ने उसी वक़्त यह भांप लिया था कि गांधीवादी “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्रवाद के नैरेटिव में ब्राह्मणवादी ताकतों की प्रवृत्तियों का अंतर्विरोध और मुस्लिमों का अलगाव शामिल है जो जिन्ना और इक़बाल दोनों के अनुसार ब्राह्मणवादी पुनुरुत्थान (एक कल्पित राष्ट्रवादी इतिहास और केन्द्रीयकरण व बहुलतावाद की प्रवृत्ति, जिसे पूंजीपतियों के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था) से बुनियादी तौर पर किसी भी तरह से अलग नहीं है। (और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें– लेखक आकार पटेल को, जिन्होंने लिखा है कि अगर भारत में वास्तविक संघीय ढाँचा अपनाया गया होता, जैसा कि जिन्ना जैसे मुस्लिम नेताओं की मांग थी, तो शायद आज हमारा वर्तमान कुछ और होता)। जिन्ना की राजनीतिक सोच में एकमात्र कमी है कि वह मुसलमानों के भीतर जाति व्यवस्था को लेकर ख़ामोश रहे। जाहिरा तौर पर इसका कारण यह है कि आसन्न अनौपनिवेशीकरण और कांग्रेस के भीतर हिन्दू एकजुटता के माहौल में उनके सामने सबसे जरूरी कार्य केंद्रीकरण और बहुसंख्यकवाद का प्रतिरोध था। इसके लिए मुसलमानों को कुछ हद तक एकजुट करना ज़रूरी था.
प्रतिनिधित्व और मुस्लिम लीग
जो बात जिन्ना के समय में एक आशंका थी, वह आज हमारे सामने कड़वी सच्चाई बनकर खड़ी है। जिन्ना के लिए, कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षतावाद असल में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के बहिष्करण और उन्हें चुप कराने का एक उपकरण था। याद करिए, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बहुसंख्यकवाद और दूसरी पहचानों को ख़त्म करने के उनके प्रयासों के बारे में ज़ोर देकर कहा था “लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर सिर्फ़ मतपेटी के ज़रिये राज करने का अधिकार मिल जाए।” जिन्ना के बारे में इतिहासकार जोया चटर्जी, अपनी किताब Shadows at Noon (पृष्ठ 67) में लिखती हैं -“1906 से लेकर अपनी मृत्यु तक, जिन्ना एक उदारवादी संविधानवादीवादी बने रहे। उनमें संवाद की असाधारण क्षमता थी। 1930 और 40 के दशक में जिन्ना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी बदली, जिसके नेतृत्व के इस दावे ने और ज़ोर पकड़ लिया कि वह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके नेतृत्व ने उन लोगों से दूरी बना ली जो इस दावे को अस्वीकार करते थे। इस अधिक प्रभुत्ववादी रुख ने जिन्ना समेत उन सभी लोगों को किनारे लगा दिया, जो यह मानते थे कि भारतीय परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा अनिवार्य है, और “भारतीयता” के अलावा भी अन्य पहचानों की मान्यता, स्थान और सम्मान होना चाहिए। अंततः, कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता असंभव हो गया, जो झुकने को तैयार ही नहीं थी, बेशक उसके सामने सर्वश्रेष्ठ समझौता वार्ता पसंद करने वाला नेता खड़ा हो।”
आप इक़बाल का 1932 में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन (All-India Muslim Conference) में दिया गया अध्यक्षीय भाषण भी पढ़ सकते हैं : “कांग्रेस के नेता यह दावा करते हैं कि वे भारत की समस्त जनता के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। लेकिन पिछले गोलमेज़ सम्मेलन ने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस सच्चाई से स्वाभाविक रूप से नाराज़ है…” इक़बाल आगे कहते हैं: “इसीलिए उन्होंने (कांग्रेस ने) आजकल एक अभियान शुरू किया है। एक ऐसे समझौते को रोकने के लिए, जिसके बारे में उन्हें डर है कि वह आने वाले संविधान में शामिल हो सकता है। वे सरकार पर यह दबाव भी बनाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों को केवल कांग्रेस के साथ ही तय किया जाए। कांग्रेस का प्रस्ताव इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि चूंकि सरकार ने महात्मा गांधी को देश का एकमात्र प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाया। एक अल्पसंख्यक समुदाय कैसे उस अभियान में शामिल हो सकता है जो उतना ही उसके ख़िलाफ़ है, जितना सरकार के ख़िलाफ़?”
1946 के चुनावों ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में अधिकांश मुस्लिम मतदाता इसी तरह महसूस करते हैं। सारे प्रान्तों में, मुस्लिम लीग ने कुल डाले गए मुस्लिम मतों का 75 प्रतिशत वोट और 87 प्रतिशत विधानसभा सीटें जीत लीं। बाद में फैलाई गई भ्रांतियों के विपरीत, यह केवल अभिजात्य वर्ग का चुनाव नहीं था। सभी पुरुषों में से 35 प्रतिशत से अधिक पंजीकृत मतदाता थे, जबकि महिलाओं में यह संख्या केवल 6–7 प्रतिशत के आसपास थी, जिससे कुल पंजीकरण आंकड़ा कुल जनसंख्या का केवल 20 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हुआ (देखें Kuwajima Sho की Muslims, Nationalism, and the Partition)। मुस्लिम लीग ने विशेष रूप से बंगाल के किसानों और मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसीडेंसी के मध्यम वर्गों में अच्छा प्रदर्शन किया। (मेरे शोध में एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटिश भारत की 4.2 करोड़ वयस्क मुस्लिम आबादी में से 60 लाख वोट पड़े, जिनमें से 45 लाख मुस्लिम लीग को मिले। मुस्लिम लीग ने 40 सीटें निर्विरोध भी जीतीं। औसत मतदान लगभग 65 प्रतिशत रहा (पंजाब के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ 16 लाख पंजीकृत मुस्लिम मतदाताओं में से 10 लाख ने मतदान किया)। इसका मतलब यह है कि कुल पंजीकृत मुस्लिम मतदाता 90 लाख से अधिक थे, जिनमें से 75 लाख से अधिक पुरुष और लगभग 15 लाख महिलाएँ थीं। इसलिए, मुस्लिम पुरुष जनसंख्या के 35 प्रतिशत से अधिक लोग पंजीकृत थे और 25 प्रतिशत से अधिक ने वास्तव में मतदान किया। (यह देखें Anwesha Roy की 2018 की पुस्तक Making Peace, Making Riots)।
इस्लाम में आधुनिकता
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आईआईटी, जेएनयू और अब तिहाड़ में बिताए इन वर्षों में मेरे अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू इस्लाम में आधुनिकता की धाराओं को समझना रहा है। ये आधुनिकता एक तरह से दो चीज़ों की प्रतिक्रिया थी पहली, मुसलमानों की राजनीतिक संप्रभुता का खात्मा, और दूसरा आधुनिक विज्ञान की ज़बरदस्त ताक़त। जेल आने से पहले मैं कट्टरपंथ पर लिख चुका था, लेकिन जेल में रहते हुए मुझे आधुनिकता के प्रति लोगों के मन में जो “रुग्ण” (pathological) प्रतिक्रियाएं हैं, उनके बारे में कहीं अधिक स्पष्टता मिली है (यहाँ “pathological” शब्द के उपयोग के लिए देखें SherAli Tareen की पुस्तक Perilous Intimacies: Debating Hindu-Muslim Friendship After Empire, 2023 का “Epilogue”)। आधुनिकता के प्रति जो यह कट्टर और लोकतंत्र विरोधी प्रतिक्रिया है, उसे केवल आधुनिक शिक्षा से नहीं, बल्कि मुस्लिम जनता की राजनीतिक एजेंसी के माध्यम से ही रोका जा सकता है। दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं।
इस्लामी देशों में राजशाही और तानाशाही ताकतें (खासकर वे जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ मिली हुई हैं) इस्लाम की लोकतंत्र–विरोधी, सांप्रदायिक और प्रतिगामी व्याख्याओं को लगातार बढ़ावा देती रहेंगी। इन प्रवृत्तियों का मुकाबला केवल एक लोकतांत्रिक, समावेशी और इन्क़लाबी इस्लाम के ज़रिए ही किया जा सकता है। ऐसा इस्लाम आधुनिक चिंतकों की सोच से प्रेरणा लेता है। विशेषकर दक्षिण एशिया में मुहम्मद इक़बाल और ईरान में अली शरीअती जैसे विचारकों से, जो अपने–अपने समाजों में इस्लामी लोकतंत्र की सबसे प्रबल आवाज़ रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ( मृत्यु – 1921) ने उस दौर को देखा जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी बुलंदी पर था। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो अंग्रेज़ी हुकूमत की विज्ञान और सियासत की कामयाबी के मुक़ाबले दिखा सकें। वह उस अलीगढ़ के प्रति भी आलोचनात्मक थे जो साम्राज्यवादी शासकों की नकल करते थे। और साथ ही वह उलेमा की उस सोच पर भी प्रहार करते थे जो आधुनिकता और नए विचारों के लिए अपने दरवाज़े बंद किए बैठी थी।
क़ुरआन बार–बार अनुभववाद, अवलोकन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की व्याख्या की प्रेरणा देता है। यहाँ तक कि प्रकृति का अवलोकन करना क़ुरआनी दृष्टिकोण में एक प्रकार की धार्मिक साधना जैसा प्रतीत होता है। इसके बावजूद, उलेमा आधुनिक वैज्ञानिक विकास के महत्व को समझने में विफल रहे (देखें: क़ुरआन, सूरा 88: आयत 17–26; सूरा 36: आयत 33–42, और इस तरह की दर्जनों अन्य आयतें; साथ ही देखें मुहम्मद इक़बाल की रचना Knowledge and Religious Experience, 1930)। लेकिन, अकबर इलाहाबादी ने इन दोनों ध्रुवों– धर्म और आधुनिकता– को जोड़ने का प्रयास किया, हालांकि, वह प्रयास निष्फल रहा। इस कोशिश में वह उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी की शुरुआत के दौर में दक्षिण एशियाई मुस्लिम चिंतन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ नुमाइंदे बन जाते हैं। वह न केवल इस्लामी ज्ञान परंपरा में पारंगत थे, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन में भी गहरी समझ रखते थे। ऐसे में वे एक विशिष्ट और बड़ी शख्सियत वाले चिंतक के रूप में उभरते हैं, जिनमें अक़ीदत तो थी, लेकिन वह उस निर्णायक बौद्धिक छलांग से चूक गए, जो ज़रूरी थी।
यह बौद्धिक छलांग अगली पीढ़ी में ही संभव हो सकी। एक ओर आधुनिकता और इस्लाम के बीच गहरे संश्लेषण का प्रयास, और दूसरी ओर भौतिकी में क्रांतिकारी विकास ने ऐसे चिंतकों को जन्म दिया – जैसे कि मुहम्मद इक़बाल। वह न केवल भौतिकवाद के विरुद्ध अधिक स्वतंत्र रूप से तर्क कर सकते थे (क्योंकि न्यूटन की भौतिकी का ढांचा टूट चुका था), बल्कि वे उन उलेमा की भी आलोचना कर सकते थे जो संदिग्ध ऐतिहासिक वृत्तांतों को पवित्र मानकर उन पर संप्रदायवाद की दीवारें खड़ी कर रहे थे। जबकि वह क़ुरआन की वास्तविक प्रेरणा और इस्लामी समुदाय के तौहीदी (एकेश्वरवादी) आधार को नज़रअंदाज़ कर रहे थे। इक़बाल का मानना था कि मुसलमानों की लोकतांत्रिक नेतृत्व व्यवस्था ऐसी संस्थाओं को जन्म दे सकती है जो इस्लामी उम्मत के जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगी। दुर्भाग्यवश, बँटवारे ने उनके इस ख़्वाब पर विराम लगा दिया। यह केवल एक अस्थायी विराम हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है।
हालाँकि, मेरे विचारों को किसी भी धार्मिक समुदाय की निंदा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा यक़ीन तार्किकता और समानुभूति का पक्षधर है। मैं अन्य धार्मिक परंपराओं में मौजूद एकेश्वरवादी और जातिविरोधी आंदोलनों का भी समर्थन करता हूँ। उदाहरण के लिए, मुहम्मद इक़बाल की गौतम बुद्ध पर कही गई यह बात देखें:
“क़ौम ने पैग़ाम-ए-गौतम की ज़रा परवा न की
क़द्र पहचानी न अपने गौहर-ए-यकदाना की”
बुद्ध ने जो संदेश दिया, उसकी क़ौम ने बिल्कुल परवाह न की!
वे अपने इस बेशकीमती मोती को परख ही नहीं सके!!
इसी तरह, इक़बाल ने गुरुनानक पर जो शब्द कहे, वे भी उल्लेखनीय हैं:
“फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से
हिंद को एक मर्द-ए-कामिल ने जगाया ख़्वाब से”
एक बार फिर तौहीद की पुकार पंजाब से उठी!
भारत को एक संत पुरुष (गुरुनानक) ने उसकी नींद से जगाया!!
मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय को अनिवार्य बनाना या किसी व्यक्ति पर नैतिक निर्णय सुनाना नहीं है। मैं महज वैचारिक श्रेणियों की चर्चा कर रहा हूँ। इस संदर्भ में मैं इक़बाल की उस बारीक और नाज़ुक सोच से सहमत हूँ, जिसे उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया:
“काफ़िर-ए-बेदार दिल पेश-ए-सनम
बेह ज़ी दीनदारी की ख़ुफ़्त अंदर हरम”
मूर्तिपूजक लेकिन जागृत और संवेदनशील हृदय वाला व्यक्ति
उस धर्मनिष्ठ व्यक्ति से बेहतर है जो हरम में भी गहरी नींद सोया हुआ है।
यदि आप यह मान बैठे हैं कि आपको सत्य का पूरा ज्ञान है, यदि आपने अपने हृदय को निष्क्रिय कर दिया है, तो आप वास्तव में तौहीद से विमुख हो चुके हैं। क़ुरआन बार–बार यह स्पष्ट करता है कि तौहीद कोई नया विचार नहीं है जिसे पैग़म्बर मुहम्मद ने शुरू किया हो, बल्कि यह तो उतना ही पुराना है जितनी स्वयं मानवता। मेरे लिए यही वह बौद्धिक उपलब्धि है जो जीवन और अध्ययन दोनों को एक सूत्र में पिरो देती है। क़ुरआन के अनुसार, हममें सबसे श्रेष्ठ वह है जो सबसे अधिक तक़वा (धर्मपरायण ) है, ना कि कोई विशेष क़बीले, धर्म या राष्ट्र का सदस्य। यही है तौहीद का विश्वदृष्टिकोण। इस पहलू की उपेक्षा ही उस घातक सोच को जन्म देती है जो दूसरों को कमतर और स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगती है। इन्हीं विचारों से मेरा मन जेल में भी भरा रहता है। मैं इन पर लिखे बिना नहीं रह सकता।
एक कप चाय
मेरे जीवन के सबसे कठिन साल मेरे पिता की मृत्यु के बाद के दो वर्ष, 2015 और 2016 रहे हैं। उन दिनों मेरी मासिक आमदनी तीस हज़ार रुपये से भी कम थी। माँ और छोटे भाई की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। हालांकि, मेरे मामा ने हर तरह से मेरा साथ दिया, फिर भी मुझे याद है, ऐसे भी दिन आए जब जेब में पाँच रुपये तक नहीं होते थे कि मैं एक कप चाय पी सकूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मेस और वहाँ के दोस्तों ने मुझे ज़िंदा रखा। मैं खास तौर पर अपने प्यारे दोस्त शफ़कत का ऋणी हूँ, जिसने मुझे अपने साथ रहने दिया। क्योंकि मैं दो बार हॉस्टल की प्रतीक्षा सूची में रह गया था। मुझे याद है, जब मेरे पिता को कैंसर का पता चला था, और फिर जब मैं एम.फिल. में दाख़िल हुआ लेकिन रहने की कोई जगह नहीं थी, तब मैं शफ़कत के साथ ही रह रहा था।
लेकिन अगले साल हालात बेहतर होने लगे। एम.फिल. के दूसरे वर्ष में मुझे मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप (2016–2021) मिल गई। 2017 में मुझे रेख़्ता में एक बेहतर फ़्रीलांस नौकरी मिल गई। वहाँ मैं सबसे बड़े उर्दू डेटाबेस के लिए एल्गोरिद्म डिज़ाइन कर रहा था। उर्दू कविता की लिप्यान्तरण (ट्रांस्लिटरेशन) और स्वचालित व्याकरणिक विश्लेषण जैसे कार्यों पर काम कर रहा था। यह मेरे लिए एक ख़्वाबों की नौकरी थी। जहाँ मेरे सारे जुनून एक जगह आ मिले थे: कोडिंग, उर्दू, कविता और इतिहास। तनख़्वाह भी पहले से बेहतर थी, और मैं आभारी हूँ निदेशक श्री संजीव सराफ़ का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मुझे सप्ताह में केवल एक दिन दफ़्तर जाना होता था, बाक़ी का सारा काम मैं बाहर से ही करता था। कुल मिलाकर, 2017 तक मेरी आमदनी स्थिर हो चुकी थी। मैं अपने परिवार को एक अच्छी राशि भेज पाता था और साथ ही अपने शोध को भी जारी रख सका। फ़ेलोशिप और रेख़्ता, इन दोनों ने मुझे अच्छी तरह से संभाल लिया।
2018 और 2019 का अधिकांश समय मैंने अपने शोध के लिए अभिलेखीय सामग्री जुटाने के लिए उत्तर भारत के शहर, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता और दिल्ली की यात्रा में बिताया। जेएनयू और वहाँ बने मेरे दोस्त मेरी बौद्धिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हालांकि मैंने वामपंथी संगठनों के ढांचे की आलोचना की, लेकिन इन संगठनों में मेरे ऐसे मित्र, कॉमरेड और चाहने वाले हैं जैसे परिवार के लोग होते हैं।
लामबंदी, क़ैद और लोकतंत्र
शाहीन बाग़ आंदोलन के शुरुआती दो हफ्तों में, आसिफ़ मुज्तबा के अलावा, वक्ताओं और भीड़ को संभालने वाले अधिकांश लोग जेएनयू के मेरे मित्र और कॉमरेड ही थे। “मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ़ जेएनयू“, एक ऐसा सामूहिक मंच था जो उस सर्वदलीय बैठक के बाद बना था, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया तय करने के लिए सबको बुलाया गया था। लेकिन उसमें केवल मुस्लिम छात्र ही पहुँचे थे जो शाहीन बाग़ आन्दोलन में पहले दिन से ही मौजूद रहे। जब वक्ताओं की ज़्यादा ज़रूरत बढ़ने लगी, तो सबसे पहले बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (BAPSA) आगे आया। इसके बाद एक वामपंथी समूह भी आया, जिसका नेतृत्व मार्तंड दा कर रहे थे, उन्होंने भी बिना शर्त समर्थन दिया। उनसे मेरी मुलाकात 2013 में जेएनयू में हुई थी। उसके बाद कई सालों तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाद में वह मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। मुझे याद है कि पाँचवें दिन मेरी आवाज़ इतनी बैठ चुकी थी कि मैं बोल नहीं पा रहा था, फिर भी गरम पानी लेकर मुझे बोलना पड़ा। यह बात कम ही की जाती है कि शाहीन बाग़ आंदोलन की स्थापना में जेएनयू की कितनी अहम भूमिका थी। वहाँ आईआईटी के कई छात्र भी थे। सबसे प्रमुख थे आसिफ़ मुज्तबा। और मैं एक तरह से जेएनयू, आईआईटी और जामिया के बीच की एक कड़ी था (मैंने जामिया से अरबी भाषा के कोर्स भी किए थे)। तो कह सकते हैं कि इन सभी कैंपसों में मेरा रहना और जुड़ाव शाहीन बाग़ की उस ऐतिहासिक सड़क नाकेबंदी का हिस्सा बनने में निर्णायक रहा, जो अब तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम घटना कही जा सकती है।
तो फिर हम जेल में क्यों हैं? और इससे हासिल क्या हुआ है? फासीवादी सत्ता हमारे जैसे लोगों को कुचलने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार, जब भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सभी संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वैधानिक रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तो जनता के पास यही एक रास्ता बचता है कि वह अपनी मौजूदगी को महसूस कराए। करोड़ो–करोड़ जनता ही असली लोकतांत्रिक ताकत हैं। यह मायने नहीं रखता कि सरल बहुमत प्रणाली (FPTP) वाली चुनाव प्रक्रिया या सत्ता के अति–केंद्रीकरण से उन्हें चुप कराया जा चुका है। अगर यदि ये व्यवस्थाएँ जनता की गरिमा और अधिकारों की सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो जनता को अपने वजूद का अहसास कराने के लिए दूसरे तरीकों से आगे आना ही होगा। यही बात शाहीन बाग़ और उसके बाद मेरे सैकड़ों भाषणों का सार रही है। जनता का जन–आंदोलन लोकतंत्र का विरोध नहीं है बल्कि यही उसकी असली परीक्षा है। एक राष्ट्र जनता का होता है, और अगर उसकी व्यवस्थाएँ और सत्ता में बैठे लोग उसके विविध समुदायों को गरिमापूर्ण जीवन देने में असफल रहते हैं, तो यह जनता का लोकतांत्रिक कर्तव्य बन जाता है कि वह उठ खड़ी हो।
बाधा डालना ही एक उपाय है जिसके जरिये जनता लोकतंत्र की स्थापना कर सकती है और प्रभावशाली हस्तक्षेप कर सकती है। मुझे यह बात बिल्कुल साफ़ नज़र आती है कि मैंने और मेरे साथियों ने प्रतिरोध की एक रचनात्मक दिशा की ओर संकेत किया था। और मुझे यह कहने में अपार ख़ुशी महसूस होती है कि लोगों ने इस आह्वान को सुना और उस पर प्रतिक्रिया दी। मुझे तब बेहद सुखद आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे भाषणों और लेखों का मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जैसे बांग्ला, तमिल और मलयालम। मेरी हैरानी की कल्पना कीजिये जब जेल में मुझे श्रीलंका की एक तमिल मुस्लिम महिला का पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि उन्हें मेरी तमिल में अनूदित तक़रीरें उनके एक सहयोगी ने तोहफ़े में दी थीं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में एक अल्पसंख्यक होने के नाते मेरे भाषणों में बहुसंख्यकवाद पर उठाए गए सवाल उनके दिल के भी क़रीब हैं। मुसलमानों और ग़ैर–मुसलमानों दोनों से ऐसे कई पत्र मुझे मिले हैं जिन्होंने मेरे भाषण (खासकर अलीगढ़ वाला) सुना या मेरे लेख पढ़े, और फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ, सराहना या आलोचना मुझे लिख भेजी। यह सब दर्शाता है कि हमारा यह पैग़ाम सीमाओं से परे जाकर पूरे दक्षिण एशिया में, हर कौम के अल्पसंख्यकों के दिल तक पहुँचा है चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू, सिख, ईसाई या कोई और जो अपने–अपने मुल्कों में बहुसंख्यावाद के शिकार हैं।
यह सब मेरे आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी है। मुझे इस बात से भी एक गहरा संतोष मिलता है कि मैंने अपने पीछे कुछ सार्थक अलफ़ाज़ छोड़े हैं जो भारत के मुसलमानों के सामने खड़े सबसे ज्वलंत और बुनियादी सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी व्यापक पहुँच और संवाद की संभावना बीस साल पहले मुमकिन नहीं थी। इंटरनेट ने, चाहे बहुत सीमित स्तर पर ही सही, ज्ञान के निर्माण और उसके साझा करने की प्रक्रिया को आज़ाद किया है। मेरे अलफ़ाज़ ज़िन्दा रहेंगे, बेशक, फासीवादी ताक़तें उन्हें मिटा देना चाहें। जैसा कि अहमद फ़राज़ ने कहा था:
“मैं कट गिरूँ कि सलामत रहूँ यक़ीं है मुझे
कि ये हिसार-ए-सितम कोई तो गिराएगा.. !!
तमाम उम्र की इन इज़ा-नसीबियों की क़सम,
मेरे कलम का ये सफ़र यूँ ही रायगां न जाएगा।”
लिखने को अब भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है।
शरजील।
शरजील इमाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस स्नातक हैं, और दक्षिण एशिया में इस्लामी इतिहास और मुस्लिम राजनीति के एक गंभीर अध्येता हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी और छात्र कार्यकर्ता रहे हैं। जनवरी 2020 में भारत के नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) के खिलाफ़ उनके भाषणों के बाद उन पर कई केस दर्ज कर लिए गए. उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। तब से उन्हें ज़मानत नहीं मिली है और उनके मुक़दमे की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। गिरफ़्तारी से पहले और बाद में, उनका लेखन TRT वर्ल्ड, द वायर, फ़र्स्टपोस्ट, द क्विंट और मकतूब मीडिया जैसे कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रकाशित होता रहा है।





